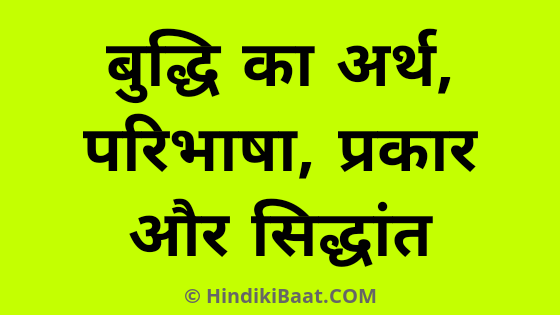संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति एवं समाज का कल्याण इसी बात में निहित है कि व्यक्तियों को अपने संवेगों को अच्छी तरह प्रयोग में लाना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संवेगात्मक परिमार्जन एवं उनकी अभिव्यक्ति के ढंग को सुधारने की आवश्यकता होती है। स्नातक स्तर में बच्चे किशोर हो जाते है एवं किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव का समय माना जाता है। इन बातों को देखते हुये इस अवस्था में संवेगों को ठीक प्रकार से प्रशिक्षित करने एवं संवेगात्मक शक्तियों को अनुकूल दिशा में प्रवाहित करने की अत्यन्त आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति का सामाजिक-आर्थिक स्तर उसके संवेगात्मक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। व्यक्ति का सामाजिक- आर्थिक स्तर उसके संवेगात्मक विकास की दिशा को निर्धारित करता है एवं उसके सकारात्मक या नकारात्मक होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
”राबर्ट के अनुसार (2001) संवेगात्मक बुद्धि मनुष्य के प्रतिदिन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।“
मनोवैज्ञानिकों ने 14 प्रकार के संवेग बताये हैं। भय क्रोध वात्सल्य, घृणा करुणा, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्मविश्वास, एकाकीपन, कामुकता, भूख अधिकार भावना, कृतिभाव, अमोद आदि। मानव जीवन में संवेगों का अत्याधिक महत्व है। यदि संवेगों का विकास संतुलित रुप से नहीं होता है, तो व्यक्ति का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। अनेक विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है। संवेगों के प्रबन्धन से ही व्यक्ति में निर्माण तथा ध्वंस की भावनायें उत्पन्न होती है। हरलॉक के अनुसार सांवेगिक वातावरण का प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है।
प्रत्येक व्यक्ति में संवेगों का स्तर भिन्न-भिन्न होता है। जो उनमें व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न करता है। सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति अपने संवेगों को नियंत्रित कर अपने व्यक्तित्व को संतुलित व समायोजित करता है तथा सामाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सावेंगिक बुद्धिमान व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों के पहचाना जाये ताकि शिक्षक तथा अभिभावक विद्यार्थियों के संवेगों को समझकर उनके सावेंगिक विकास में सहायक सिद्ध हो सके। विद्यार्थी परस्पर एक-दूसरे के संवेगों को समझकर समुचित समायोजन कर सके। स्टीव हीन के अनुसार ‘‘संवेगात्मक बुद्धि संवेगों को महसूस करनें, उपयोग करने, सम्प्रेषित करने, पहचानने, स्मरण करने उनसे सीखने उनका प्रबन्धन करने व समझने की जन्मजात क्षमता है।’’
प्राचीन भारत में शिक्षा को व्यक्ति का सर्वांगीण विकास का एक साधन माना जाता था। शिक्षा तथा विद्या ज्ञान की एक दूसरे के पर्याय के रूप में जाना जाता था तथा विद्या विहिन व्यक्ति को पशु तुल्य माना जाता था। कालान्तर में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। (ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्र) तथा मोक्ष उनके जीवन का उद्देश्य बन गया और ऐसी विद्या को आवश्यकता महसूस की गई जो उन्हें मुक्ति प्रदान करें। (सा विद्या या विमुक्तये) इस प्रकार विद्या जो शिक्षा का पर्याय भी लोगों के भौतिक तथा नैतिक कल्याण के साथ-साथ मोक्ष के लिए तैयार करने का साधन बन गई। शिक्षा के बारे में ढेर सारी चर्चाएं हो गयी है हम थोड़ा सा अब शिक्षा मनेविज्ञान के बारे में चर्चा करते है क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि का तात्पर्य कहीं न कहीं से शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और यह सही भी है। विज्ञान की जो भूमिका हमारी आम जिन्दगी में होती है। वही भूमिका शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में निभाई जाती है। बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाकर उन्हें व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही किसी भी शिक्षण व्यवस्था का परम लक्ष्य होता है। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया। दूसरी अवस्था में मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान कहा जाने लगा। तृतीय अवस्था में मनोविज्ञान को आत्मा तथा मन के स्थान पर चेतना का विज्ञान अथवा चेतन व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित करने के प्रयत्न प्रारम्भ हुए।
मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञानमयी है क्योंकि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में आज सर्वमान्य रूप से मान्यता प्रदान की जा चुकी है।मनोविज्ञान सभी प्राणी मात्र के सम्पूर्ण व्यवहार के अध्ययन से अपना सम्बन्ध रखता है। अध्ययन किया जाने वाला यह क्षेत्र अपने आप में काफी विस्तृत है। इसका अनुमान जिसके व्यवहार का मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है और जिस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन होता है इन दोनों पक्षों की विस्तृत की व्याख्या के आधार पर सहज ही लगाया जा सकता है।
शिक्षा मनोविज्ञान के बाद अब हम बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। पशुओं की तुलना में मनुष्य को कई ज्ञानात्मक योग्यताओं से सम्पन्न माना जाता है जो उसे विवेकशील प्राणी बनाती है, वह तर्क कर सकता है। भेद कर सकता है, समझ सकता है और नई स्थिति का सामना भी कर सकता है। निश्चित रूप से वह पशुओं से श्रेष्ठ है, परन्तु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। व्यापक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है।
बुद्धि का अर्थ
उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है जो जीवन की सामान्य स्थितियों का सामना करने में सफल हो। ‘बुद्धि’ में ऐसी कौन सी चीज है? मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। बुद्धि की कई परिभाषाएं है जो निम्नलिखित है-
1. वुडवर्थ और मार्किवस- ”बुद्धि का अर्थ प्रतिभा का प्रयोग करना। किसी स्थिति का सामना करने या किसी कार्य को करने के लिए प्रतिभात्मक योग्यताओं का प्रयोग बुद्धि है।“
2. स्टर्न- ”बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिन्तन करता है। जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आपको ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता ”बुद्धि“ कहलाती है।“
3. टरमैन- ”व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिन्तन करता है, उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है।“
4. वैगनन- ”अपेक्षाकृत नई एवं पविर्तित स्थितियों को समझने तथा उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता ‘बुद्धि’ है।“
5. डैविड वैक्सलर- ”बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। विवेकपूर्ण चिन्तन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंगसे सामना करता है।“
बुद्धि की प्रकृति या स्वरूप
मनोविज्ञान की उत्पत्ति से लेकर आज तक श्बुद्धि का स्वरूपश् निश्चित नहीं हो पाया है। समय.समय पर जो परिभाषाएँ विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की जाती रहींए वह इसके एक पक्ष या विशेषता या क्षमता से सम्बन्धित थीं। अतरू आज तक उपलब्ध सामग्री के अधार पर बुद्धि का स्वरूप तथा इसकी प्रकृति क्या हैघ् बुद्धि की प्रकृति या स्वरूप का वर्णन हम निम्न प्रकार से करेंगे.
सीखने की योग्यता
भारतीय मनीषियों एवं ऋषियों ने श्ज्ञानश् को जीवन का प्रमुख साधन एवं साध्य माना है। अतरू जो व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण कर लेता हैय उसे समाज उच्च स्थान देता है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिक से अधिक ज्ञान को ग्रहण करने वाली योग्यता को ही श्बुद्धिश् माना है।
जैसा कि श्डियर वानश् ने लिखा है. ष्बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है
समस्या समाधान की योग्यता
प्रत्येक व्यक्ति को विकास के साथ.साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है। जो व्यक्ति इन समस्याओं पर जितनी शीघ्र विजय प्राप्त कर लेता है या उनसे छुटकारा प्राप्त कर लेता हैए वही सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है। अतः समस्या समाधान में प्रयोग की गयी योग्यता ही श्बुद्धिश् है।
जैसा रायबर्न ने लिखा है. ष्बुद्धि वह शक्ति हैए जो हमको समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है
अमूर्त चिन्तन की योग्यता
प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार से चिन्तन प्रक्रिया को अपनाता है। प्रथम.मूर्त रूप से चिन्तन करके ज्ञान प्राप्त करना और द्वितीय.अमूर्त रूप से चिन्तन करके। अमूर्त रूप से तात्पर्यए जो चीजें हमारे समक्ष नहीं हैं उनका कल्पना तथा स्मृति के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। अतरू अमूर्त चिन्तन में जो व्यक्ति अधिक सफल होता हैए उसे बुद्धिमान कहा जाता है।
जैसा कि टरमैन ने कहा है. ष्एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता हैए जितनी उसमें अमर्त चिन्तन की योग्यता होती है
पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता ;
प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विकास करता है। विकास के समय सफलताएँ और असफलताएँ दोनों ही आती हैं। जो व्यक्ति दोनों में समाजीकरण एवं सामंजस्य करते हुए विकास करता हैए उसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है या जो जितनी शीघ्र पर्यावरण को अपने अनुक्ल कर लेता है।
जैसा कि विलियम स्टर्न ने लिखा है. ष्जीवन की परिस्थितियों और नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन ही बुद्धि है
बुद्धि कितने प्रकार की होती है
बुद्धि कितने प्रकार की होती हैघ् बुद्धिमत्ता कितने प्रकार की होती है बुद्धिमता कितने प्रकार की होती है विविध बुद्धिमत्ता कितने प्रकार की होती है बुद्धि परीक्षण के प्रकार बुद्धि के प्रकारए बुद्धि क्या हैए विविध बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के अनुसार कुल कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है
थार्नडाइक के अनुसार. बुद्धि अनेक प्रकार की शक्तियों का समूह हैए इसलिये उन्होंने स्थूल दृष्टि से बुद्धि के तीन प्रकार बताये.
1 अमूर्त बुद्धि
2 सामाजिक बुद्धि
3 यान्त्रिक बुद्धि
अमूर्त बुद्धि
पुस्तकीय ज्ञान के प्रति अपने को व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि है। शाला में बुद्धि परीक्षाओं द्वारा बालकों की विशिष्ट योग्यताए रुचिए रुझान एवं प्रवृत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके द्वारा पढ़ने
लिखने प्रतीकों एवं सूत्रों का हल तथा अन्य समस्याओं का हल आसानी से किया जा सकता है। ज्ञानोपार्जन श्बुद्धिश् पर निर्भर करता है।
अमूर्त बुद्धि त्रिमुखी है। स्तरए क्षेत्र और वेग अथवा गति ही उसकी तीन विभिन्न क्रियाएँ हैं। कठिनाई स्तर को समझनाए कार्य की सक्षमता का आभास करना तथा कार्य करने की गति को समझना है।
सामाजिक बुद्धि
अपने समाज के अनुकूल व्यवस्थित करने की योग्यता ही सामाजिक बुद्धि कहलाती है। परस्पर सद्भावए सहयोगए सद्व्यवहार तथा अन्य रुचि के साथ सामाजिक कार्यों में भाग लेनाएश्सामाजिक बुद्धिश्है।जीवन की सफलता के लिये श्सामाजिक बुद्धिश् का ज्ञान एवं प्रयोग आवश्यक है।
यान्त्रिक बुद्धि
व्यक्ति में यह योग्यता यन्त्री तथा मशीनों के साथ अनुकूलन की योग्यता है। इस योग्यता या दक्षता के आधार पर व्यक्ति कुशल कारीगरए चालकए मिस्त्री या इन्जीनियर बन सकता है। इस प्रकार वह इन परिस्थितियों मेंए जिनका सम्बन्ध यन्त्रों एवं भौतिक पदार्थों से होता हैए अपने को समायोजित एवं सुव्यवस्थित कर लेता है।
इस दक्षता को अभ्यास द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इस दक्षता के अभाव में व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाता तथा दब्बू व्यक्तित्व का व्यक्ति रह जाता है।
बुद्धि एवं योग्यता
बुद्धि की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिये यह जानना भी आवश्यक है कि बुद्धिए कौशल ;ैापससद्ध नहीं होती और न ही स्मृति या प्रतिभा होती है। यहाँ तक कि ज्ञान को भी बुद्धि नहीं कहा जा सकता। बुद्धि अमूर्त ;।इेजतंबजद्धए यान्त्रिक और सामाजिक होती है।
वेशलर ने बुद्धि में इन योग्यताओं को सम्मिलित किया है.
उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता।
तर्कपूर्ण चिन्तन करने की योग्यता।
वातावरण में प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करना।
अतः इस विचार के अनुसार बुद्धि इन तत्त्वों की एक संयुक्त योग्यता होती है। बुद्धि का रुचिए अभिवृत्तिए प्राप्त ज्ञान एवं कौशल के साथ सफलता प्राप्त कराने में प्रमुख योगदान रहता हैए इसे विवेक भी कहा जा सकता है।
बुद्धि की विशेषताएं
1 बुद्धि जन्मजात प्राकृतिक शक्ति है।
2 प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दूसरे से भिन्न होती है।
3 यह व्यक्ति के सीखने और समायोजन स्थापित करने में सहायता करती है।
4 यह व्यक्ति को कठिन समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करती है।
5 वंश का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है।
6 वातावरण प्रशिक्षण और शिक्षा भी बुद्धि को प्रभावित करती है।
7 लिंग की भिन्नता के कारण बुद्धि में भिन्नता नहीं आती।
बुद्धि के सिद्धान्त
एक कारक सिद्धान्त-
इस सिद्धान्त के अनुसार ‘बुद्धि’ में केवल एक प्रतिभात्मक क्षमता सम्मिलित होती है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं में विद्यमान होती है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन कसरे फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेको जाता है। बाद में अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों टर्मन एवं स्टर्न तथा जर्मन वैज्ञानिक एबिंगास ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुुद्धिवह शक्ति हैं जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। यह समग्र ;सभीद्ध ग्रुप वाली बुद्धिएक समय में व्यक्ति को एक ही कार्य करने के लिए अग्रसर करती है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि यदि एक व्यक्ति किसी एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्र में भी निपुण होगा। डॉक्टर जानसन जो कि इस सिद्धांत से सहमत थेए उनका विश्वास था कि बुद्धि वह उच्च मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति के समस्त मानसिक गुणों का संचालन होता है।
बहु कारक सिद्धान्त-
इस सिद्धान्त के मुख्य समर्थक थार्नडाइक थे। इस सिद्धान्त के अनुसार ‘बुद्धि’ कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती बल्कि ‘बुद्धि’ में कई स्वतन्त्र, विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है। जो विभिन्न कार्यों को सम्पादित करती है। इस सिद्धांत को मूल मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं।
थार्नडाइक ने स्पीयर मैन के सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक को नकारते हुए मानसिक योग्यताओं की व्याख्या में मूल कारकों ;चतपउंतल ंिबजवतद्ध एवं सामान्य कारकों का उल्लेख किया। इनका वर्णन इस प्रकार है
ण्मूल कारकों
थार्नडाइक के अनुसार विभिन्न मानसिक योग्यताएं जैसे आंकिक योग्यता ;दनउमतपबंस ंइपसपजलद्धए शब्द प्रवाहए दैनिक योग्यतातार्किक योग्यतास्मृतिशाब्दिक योग्यता आदि व्यक्ति के समस्त मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। उनके अनुसार या आवश्यक नहीं है कि यदि व्यक्ति एक विषय में योग्य हो तो दूसरे विषय में योग्य होगा।
ण्सामान्य कारकों
जब दो मानसिक क्रियाओं के प्रतिपादन में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है यह निश्चित हो जाता है कि यहां पर सामान्य कारक उपस्थित है। सामान्य कारक की मात्रा उनके साथ संबंध की मात्र से प्रदर्शित होता है। दूसरे शब्दों में जैसे कि चित्र में दिखाया गया है दो या दो से अधिक मूल्य कारक आपस में मिलकर संयुक्त रूप से किसी मानसिक क्रिया को प्रभावित करते हो तो वहां पर जो संयुक्त भाग यह संबंधित भाग होता है व सामान्य कारक कहलाता है।
बुद्धि के सिद्धान्त बुद्धि की संरचना यानी बुद्धि में निहित तत्वों अथवा कारकों के बारे में बताते है। जैसे बुद्धि का एक कारक सिद्धान्त यह बताता है कि व्यक्ति विशेष की बुद्धि में केवल एक ही कारक अथवा तत्व होता है जिसे बौद्धिक क्षमता का नाम दिया जा सकता है। सभी बौद्धिक क्रियाओं को सम्पन्न करने में यही एक कारक या तत्व हर समय उपस्थित रहता है। इसके ठीक विपरीत बुद्धि का बहुकारक सिद्धान्त यह बताता है कि बुद्धि एक नहीं अनेक तत्वों से मिलकर बनी है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है जिनकी मदद से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के विशिष्ट एवं सूक्ष्म कार्यों को संपादित कर सकते है।
द्विकारक सिद्धान्त
स्पीयर मैन के द्वारा 1904 ईस्वी में दो कारक बुद्धि सिद्धांत दिया गया। स्पीयर मैन के अनुसार बुद्धि के सिद्धांत की संरचना के दो कारक इस प्रकार है.
१ण् सामान्य कारक २ण् विशिष्ट कारक
स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धान्त अपने नामानुसार यह बताता है कि बुद्धि में एक नहीं बल्कि दो तत्वों का कारकों का समावेश होता है जिन्हें सामान्य बुद्धि या विशिष्ट बुद्धि के नाम से जाना जाता है। सामान्य बुद्धि जहाँ सामान्यतः सभी मानसिक कार्यों को करने में अपना योगदान देती है वही विशिष्ट बुद्धि का उपयोग विशिष्ट कार्यों को करने में होता है।इस तरह से किसी एक मानसिक कार्य को करने हेतु सामान्य बुद्धि तथा विशिष्ट बुद्धिसेयुक्त दोनों ही प्रकार के तत्वों या कारकों की आवश्यकता पड़ती है।
सामान्य कारक
सामान्य कारक को स्पष्ट करते हुए स्पीयर मैन ने कहा है कि यह एक जन्मजात कारक होता है तथा वयक्तिक विभिन्नता के आधार पर अलग.अलग व्यक्तियों में अलग.अलग मात्रा में पाया जाता है। जिस व्यक्ति में सामान्य कारक जितना अधिक होता है वह व्यक्ति मानसिक कार्य करने में उतना ही योग्य होता है। स्पीयर मैन ने अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि समस्त मानसिक क्रियाएं कुछ सीमा तक सामान्य कारकों पर निर्भर करती हैए तथा दो मानसिक क्रियाओं में जितना अधिक सहसंबंध पाया जाता है उतनी ही मात्रा में सामान्य कारक के उपस्थित होने की बात की जाती हैं।
सामान्य कारक की विशेषताएं
सामान्य कारक सभी व्यक्तियों में निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं।
ये जन्मजात होते हैं उन्हें अर्जित नहीं किया जा सकता है।
विषयों का स्थानांतरण सामान्य कारक के द्वारा ही होता है।
दर्शन सामान्य विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के सीखने में सामान्य कारक महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।निम्न चित्र में इसे ळ से दर्शाया गया है.
संवेगात्मक विकास मानव बुद्धि और विकास का महत्वपूर्ण पहल है। प्रेम, क्रोध, भय, घृणा आदि संवेग बच्चे के व्यक्तित्व और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार केवल उसकी शारीरिक बुद्धि और विकास को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सौन्दर्य बोध के विकास पर भी यथेष्ठ प्रभात डालता है। संवेगों की मानव जीवन में इस बहुमुखी उपयोगिता के कारण उनके बारे में पूरी तरह जानना अति आवश्यक हो जाता है। संवेग क्या है? इनका उद्गम क्या है? इनका विकास कैसे होता है? व्यक्ति को यह किस तरह प्रभावित करते हैं?
विशिष्ट कारक
व्यक्ति कई प्रकार के मानसिक क्रियाएं करता है इन मानसिक क्रियाओं में कुछ कारक ऐसे हैं जो मानसिक क्रिया एक में होने पर दूसरी में नहीं पाई जाती अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भिन्न.भिन्न प्रकार के विशिष्ट कारक उपस्थित होते हैं। उपरोक्त चित्र में विशिष्ट कार को को ै1एै2ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ै4 से प्रदर्शित किया गया हैए यह दर्शाता है की अलग.अलग विशेष कार्यों के लिए अलग.अलग विशिष्ट कारकों की आवश्यकता होती है। ये विशिष्ट कारक किसी व्यक्ति में एक होते हैं तो किसी में एक से अधिक।
स्पीयर मैन के अनुसार विशिष्ट कारक की विशेषताएं इस प्रकार हैरू.
पण् सामान्य कारकों की तरह जन्मजात न होकर अर्जित होते हैं
पपण् व्यक्ति में विशिष्टकों की मात्रा निश्चित नहीं होतीए यह कम या ज्यादा हो सकती है।
पपपण् इस कारक को प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
पअण् कला हस्तकला संगीत नृत्य तथा गायन जैसे विषयों में विशिष्ट कारक आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं।
इस प्रकार बुद्धि;पदजमससपहमदबमद्ध के दो कारक सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में सामान्य कारक ळ की आवश्यकता होती है और विभिन्न मानसिक क्रियाओं में विभिन्न विशिष्ट कारकों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। कुछ मानसिक क्रियाओं में सामान्य कारक महत्वपूर्ण होते हैं तो अन्य में विशिष्ट कारक। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी विषय के सीखने में दोनों कारकों का होना अनिवार्य है।
गिलफोर्ड का त्रि.आयाम बुद्धि सिद्धान्त
इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत या एस आई मॉडल के नाम से जाना जाता है गिलफोर्ड 1966 तथा उनके साथियों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
उनके अनुसार मनुष्य की मानसिक क्रियाओं में अनेक विमाएं पाई जाती हैए लेकिन इसके बावजूद इस समानता के आधार पर तीन विमाओं संक्रियाविषय वस्तु तथा उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धिकी यह तीनों विमाएं पर्याप्त रूप से भिन्न है। इनका पृथक पृथक वर्णन इस प्रकार है.
संक्रिया
संक्रिया का तात्पर्य प्राणी के द्वारा के किये जाने वाले मानसिक क्रियाओं के स्वरूप से है। गिलफोर्ड महोदय ने इस आधार पर मानसिक क्रियाओं को पांच भागों में बांटा है जो इस प्रकार है.
मूल्यांकन
मूल्यांकन का अर्थ प्राणी की उस कार्य क्षमता से है जिसके आधार पर वह सभी पक्षों को ध्यान में रखकर निर्णय करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है।
अभिसारी चिंतन
अभिसारी चिंतन में प्राणी की चिंतन प्रक्रिया केंद्र की ओर उन्मुख होती है। अर्थात वह लीक से न हटकर परंपरागत मूल्य तथा मान्य सूचनाओं को प्रस्तुत करती है।
अपसारी चिंतन
अपसारी चिंतन में चूंकी प्राणी केंद्र से विमुख विभिन्न दिशाओं से सोचता है तथा कुछ विविधता तना नवीनता को हासिल करने का प्रयास करता है अतः सृजनात्मकता से इसका घनिष्ठ संबंध होता है।
स्मृति
स्मृति एक प्रमुख मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सीखी गई या अनुभव की गती सामग्री को धारण करके रखा जाता है तथा समय आने पर उसका उपयोग किया जाता है।
मद्ध संज्ञान
यह सीखने या अधिगम की महत्वपूर्ण संक्रिया है इसमें चिन्हों संकेतों तथा भाषा के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
विषय वस्तु
इसके अंतर्गत बुद्धि; के विभिन्न कारको को इस आधार पर किया गया है कि बुद्धि के प्रमुख विषय वस्तु या सामग्री क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रमुख रूप से चार प्रकार की विषय वस्तु मानी गयी है। जो इस प्रकार है.
आकृतिक
आकृतिक विषय वस्तु को आंखों से देख कर पहचाना जा सकता है क्योंकि इसका उद्देश्य स्वयं को प्रदर्शित करना मात्र होता है । यह विभिन्न आकारए रंगए रूप में नजर आती है।
सांकेतिक
सांकेतिक विषय वस्तु में प्रायः शब्दों अंकू तथा परंपरागत चिन्हों का प्रयोग होता हैए जोकि सामान्यतः अल्फाबेट या अंको की पद्धति के रूप में व्यवस्थित होते हैं।
शाब्दिक
बुद्धि का या भाषिक पक्ष होता है। इसमें भाषा या शब्द अपना अर्थ या विचार स्वयं प्रकट करते हैं।
व्यवहारिक
प्राणी का समस्त व्यवहार किसी न किसी रूप में प्राणी की बुद्धि को प्रदर्शित करती हैं अतः यह बुद्धि;की एक प्रमुख विषय वस्तु है।
ण्उत्पादन
उत्पादन का अर्थ किसी विषय वस्तु के द्वारा की गयी संक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न उत्पादों से है। इनके छह प्रकार बताएं गए हैं तथा सभी कारक विश्लेषण पर आधारित होते हैं। उत्पादन निम्न प्रकार से हैं
इकाइयां
वर्ग
संबंध
पद्धतियां
स्थानांतरण
ण्अपादन
बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत
अन्य नाम . त्रिविमीए सिद्धांत त्रिअंशीय सिद्धांतध् बुद्धि संरचना सिद्धांत . बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक जे पी गिलफोर्ड
थे गिलफोर्ड ने 1967 में एक डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि का सूचना मॉडल के नाम से जाना जाता हैण् इस मॉडल के अंतर्गत 5 × 4 × 6 त्र 120 कारक बनाये हुए हैं
गिलफोर्ड ने बुद्धि की इकाइयों को 3 विमाओ में बांटा था
;1द्ध सक्रिय प्रक्रिया .समस्या समाधान के लिए जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता हैण् उसे ही हम सक्रियाध् प्रक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैंण् सक्रिया आयाम में कुल 5 भाग बताए गए हैं
1ण्स्मृति धारण
2ण्संज्ञान
3ण्अभिसारी
4ण्अपसारी
5ण्मूल्यांकन
6ण् स्मृति अभिलेख
सक्रिया में कुल भागों की संख्या 6 होती है
; विषय वस्तु ध्अंतर्वस्तु . हमें समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती हैण् उसे ही हम विषय वस्तु के नाम से जानते हैंण् विषय वस्तु आया में कुल चार भाग होते हैंण्
1ण्प्रतीकात्मक
2ण् शाब्दिक
3ण् आकृति
4ण्आत्मक व्यवहारिक
विषय वस्तु के अंदर आत्मक व्यवहारिक को हटाकर इसमें दृष्टि और श्रवण भाव को सम्मिलित किया गयाण् और इनकी संख्या पांच कर दी गई
;उत्पादध् परिणाम.
हमें समस्या के समाधान के जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैण् उसे ही हम उत्पादध्परिणाम कहते हैंण् उत्पाद आयाम मे कुल 6 भाग बताएंण्
1ण्इकाई
2ण् वृद्ध
3ण् संबंध
4ण्रूपांतरण
5ण् पद्धति
6ण्अनुप्रयोग
गिलफोर्ड के अनुसार . ; 5 × 4 × 6=120
संशोधित मॉडल . प् त्र व् × ब् × च् ; 5 × 5 × 6=150
वर्तमान में संशोधित मॉडल . ; 6 × 5 × 6= 180
थस्टर्न का समूह कारक सिद्धांत
यह सिद्धांत स्पीयर मैन द्वि कारक तथा थार्नडाइक के बहु कारक सिद्धांतों के बीच का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि न केवल सामान्य कारकोका प्रदर्शन है और न ही विभिन्न विशिष्ट कारकों काए बल्कि मूल कारकों के समूह के आधार पर बुद्धि के मानसिक कार्य होते हैं।
थस्टर्न महोदय के अनुसार बुद्धि का निर्माण कर लेते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की बुद्धि को दर्शाते हैं। ये मूल कारकइस प्रकार है शाब्दिक योग्यता आंकिक योग्यतादैशिक योग्यता शब्द प्रवाह तर्कशक्ति तथा स्मृति निम्न चित्र में दर्शाया गया है कि ये कारक किस प्रकार समूह का निर्माण करते हैं।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बुद्धि विभिन्न समूह में पाई जाने वाली अनेक प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है। यद्यपि मानसिक योग्यताएं क्रियात्मक रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होती है फिर भी एक ही समूह की योग्यताओं में परस्पर समानता या सहसंबंध पाया जाता है।
पियाजे का मानसिक बुध्दि का सिद्धांत
पियाजे के अनुसार बुद्धिएक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतरू क्रियाएंसम्मिलित होती है। इनके अनुसार जैसे.जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होते जाता है वैसे वैसे उनका बौद्धिक विकास भी होते जाता है।
ष्पियाजे के विचार में बुद्धि एक ऐसे अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता का पारंपारिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गयी अन्तरू क्रिया दोनों ही सम्मिलित होती हैं। उनके अनुसार बौद्धिक विकास कुछ संज्ञानात्मक क्रियाओंजैसे प्रकृति के नियम को समझना व्याकरण के नियम को समझना तथा गणितीय नियमों को समझना आदि के विकास पर निर्भर करता है।
पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत
पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं वर्नन ने दिया था मनोवैज्ञानिकों ने स्पीयर मैन ळ कारक सिद्धांत के तत्व थस्टर्न के समूह कारक सिद्धांत के तत्वों तथा बहु कारक सिद्धांत के तत्वों को एक साथ मिलाकर बुद्धि के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे पदानुक्रमिक सिद्धांतकी संज्ञा दी गई है।
पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि को एक पिरामिड से तुलना किया गया जिसमें बुद्धि के भिन्न.भिन्न तत्वों या कारको को एक पदानुक्रम के रूप में व्यक्त किया गया। पिरामिड के सबसे ऊपरी स्तर पर स्पीयरमैन के ळ कारक को रखा गया जिसकी जरूरत सभी तरह के बौद्धिक या मानसिक कार्य को करने में होती है पदानुक्रम के दूसरे स्तर पर थस्टर्न के समूह कारकके समान दो विस्तृत समूह कारक होते हैं एक शाब्दिक शैक्षिक कारक तथा दूसरा व्यापारिक यांत्रिक कारक फिर इन दो प्रमुख समूह कार को को तीसरे स्तर पर अन्य छोटे.छोटे समूह कारकों में बांटा गया है। जो गिलफोर्ड के बहु कारक के समान है। उसी तरह व्यवहारिक यांत्रिक कारक को यांत्रिक कारकए स्थानिक कारक मैचुअल कारक आदि में बांटा गया है। आगे विश्लेषण करके फिर इन कारको को भी छोटे.छोटे उपकार कारकों में बांटा जा सकता है। पदानुक्रम सिद्धांत के सबसे निचले स्तर पर स्पीयर मैन का ै कारक होता है जिसके द्वारा एक ऐसी क्षमता का बोध होता है जिसकी जरूरत सिर्फ एक खास मानसिक कार्य में ही होती है।
इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्धिके पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि को एक ऐसा पदानुक्रम मॉडलके रूप में व्यक्त किया गया है जिसका आकार एक वंश वृक्षके समान होता है जहां ळ कारक सबसे ऊपरी सतह पर तथा ै कारक सबसे निचली सतह पर तथा अन्य संकीर्ण समूह कारको को इन दोनों के बीच में रखा गया है।
संवेग क्या है?
संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से मानी जाती है जो उत्तेजित करने ‘हलचल मचाने’, ‘उथल-पुथल’ या ‘क्रान्ति उत्पन्न करने’ जैसे अर्थों में प्रयुक्त होता है।
वुडवर्थ- ”संवेग किसी प्रणाली की गतिमय और हलचल अवस्था है। व्यक्ति को स्वयं यह अपनी भावनाओं को उत्तेजनापूर्ण स्थिति प्रतीत होती है। दूसरे व्यक्ति को यह उत्तेजित अथवा अशांत मांसपेशियों और ग्रंन्थियों की एक क्रिया के रूप में दिखाई देती है।“
क्रो व क्रो- ”संवेग वह भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था या सामान्यीकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है और जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाह्य व्यवहार द्वारा होती है।“
मॅकडूगल- ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेगों को जन्म देने वाला कहा है। उनके अनुसार मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार के तीन पक्ष होते हैंः
1. ज्ञानात्मक पक्ष
2. भावात्मक पक्ष
3.क्रियात्मक पक्ष
उदाहरण के रूप में जब बच्चा किसी साँड को अपनी ओर आता हुआ देखता है तब उसके मूल प्रवृत्तिजन्य व्यवहार में उपरोक्त तीनों पक्ष देखने को मिलते है। पहले तो वह सांड का प्रत्यक्षीकरण करता है। यह जानकर की यह सांड है उसे भय नामक संवेग की अनुभूति होती है। इस अनुभूति के परिणामस्वरूप वह भाग कर अपनी प्राण रक्षा करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार के उदाहरणों के आधार पर मॅकडूगल ने यह निष्कर्ष निकाला कि मूल प्रवृत्तिजन्य उत्तेजना के समय होने वाली भावात्मक अनुभूति को ही संवेग कहा जाता है।
संवेगों की विशेषताएँ
संवेगों की उत्पत्ति उनके द्वारा शरीर में होने वाले आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन और व्यवहार को दिशा प्रदान करने सम्बन्धी बातों को लेकर उनकी प्रकृति जन्य विशेषताओं के बारे में निम्न बातों कहीं जा सकती है-
1. संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ कोई न कोई मूल प्रवृत्ति अथवा मूलभूत आवश्यकता जुड़ी रहती है। जब मूलभूत आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होती है अथवा उसकी सन्तुष्टि में बाधा पड़ती है तो उस समय संवेग अपना-अपना कार्य प्रारम्भ कर देते हैं।
2. सामान्य रूप से संवेग की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होती है। किसी भी संवेगात्मक अनुभूति के लिए पदार्थ या परिस्थिति के रूप में किसी सशक्त उद्दीपक की आवश्यकता होती है। शरीर में होने वाले सभी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तनों द्वारा संवेगों की मात्रा और गति दोनों में ही तीव्रता आती है।
इन विशेषताओं के अतिरिक्त संवेगों के सम्बन्ध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें है जो निम्न हैं-
(1) प्रत्येक जीवित प्राणी को संवेगों की अनुभूति होती है।
(2) व्यक्ति को अपनी वृद्धि और विकास की हर अवस्था में इनकी अनुभूति होती है।
(3) सभी व्यक्ति संवेगात्मक रूप से एक जैसे नहीं होते। संवेगों की मात्रा और अभिव्यक्ति के ढंग से पर्याप्त अन्तर पाया जाता है।
(4) एक ही संवेग विभिन्न प्रकार के उद्दीपन, चेष्टाओं, वस्तुओं और क्रियाओं के द्वारा जागृत किया जा सकता है।
सभी प्रकार के संवेगों को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा जासकता है। इनमें से एक को साकारात्मक संवेग तथा दूसरे को नकारात्मक संवेग का नाम दिया जाता है।
1.1.6 विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास
विकास अपने सामान्य रूप में आयु बढ़ने के साथ-साथ होने वाले परिवर्तनों का ही दूसरा नाम है।जन्म के पश्चात् बच्चे में धीरे-धीरे विभिन्न संवेगों का जन्म होता रहता है। बचपन में संवेगों को जागृत करने वाले उद्दीपक की प्रवृत्ति में भी बाद में पर्याप्त अन्तर आता चला जाता है।संवेगों के अभिव्यक्त करने का ढंग भी परिवर्तित हो जाता है। विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संवेगात्मक विकास का निम्नलिखित रूप में वर्णन किया जा सकता है।
(अ) शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास- (1) अपने जन्म के समय से ही अपनी चीख पुकार और हाथ पैर चलाने के द्वारा बच्चा अपने अन्दर संवेगों की उपस्थिति का आभास देता है।
(2) श्रीमती हरलाक लिखती है- ”जन्म के समय और उससे कुछ देर बाद संवेगात्मक व्यवहार के प्रथम दर्शन शक्तिशाली उद्दीपकों के प्रति सामान्य उत्तेजना के रूप में होते हैं। इस समय शिशु में कोई ऐसे स्पष्ट निश्चित संवेगात्मक पैटर्न का पता नहीं चलता जिन्हें विशेष संवेगात्मक अवस्थाओं के रूप में पहचाना और जाना जा सकता हो।“
(3) स्प्टिज के अनुसार सामान्य उत्तेजना की आनन्ददायक तथा विषादमय दो प्रकार की अलग-अलग अनुक्रियाओं की अभिव्यक्ति निम्न प्रकार से होती है- ”पहले दो मास में शारीरिक उद्दीपकों द्वारा हर्ष और विषाद की उत्पत्ति होती है। तीसरे माह में बड़ों के हंसने और उनसे खेलने के परिणामस्वरूप वह मुस्कुराने का प्रयास करता है और इस तरह मनोवैज्ञानिक उद्दीपन के फलस्वरूप उसमें आनन्दमयी अनुक्रिया होती है। कुछ समय बाद यह देखा जाता है कि अगर शिशु को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह बहुत दुःखी होकर रोने लग जाता है और इस तरह से मनोवैज्ञानिक उद्दीपकों के माध्यम से उसमें विषाद की उत्पत्ति होने लगती है।
(ब) बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास- बाल्यावस्था के प्रारभ काल तक बच्चे में प्रायः सभी संवेगों का जन्म हो चुका होता है। अतः बाल्यावस्था में कोई नवीन संवेगों की उत्पत्ति न होकर संवेग जागृत करने वाली परिस्थितियों और उद्दीपकों की प्रकृति और संवेगों को अभिव्यक्त करने के ढंग में परिवर्तन होते रहते है।
1. शैशवावस्था में बच्चा बहुत स्वार्थी होता है। वह अपनी ही हित साधना में लीन रहता है। लेकिन जैसे-जैसे वह बड़ा होता चला जाता है उसकी दुनिया भी बड़ी होती जाती है और अब उसके संवेग अनेक प्रकार के उद्दीपकों और परिस्थितियों द्वारा जागृत होना प्रारम्भ कर देते हैं।
बाल्यावस्था में बालक को अपनी भावनाओं के प्रकाशन के लिए भाषा का माध्यम मिल जाता है, अब वह अधिक सामाजिक हो जाता है और यह अनुभव करने लगता है कि अब उसे डरना या बातचीत में रोना अथवा गुस्सा होना शोभा नहीं देता। उसमें बुद्धि का पर्याप्त विकास हो जाने के कारण अब वह अपने संवेगात्मक उफान पर नियन्त्रण स्थापित करने में समर्थ बन जाता है।
(स) किशोरावस्था में संवेगात्मक बुद्धि- किशोरावस्था में संवेगात्मक बुद्धि में अनेक परिवर्तन आते है। वास्तव में किशोरावस्था का आगमन संवेगात्मक बुद्धि में और तीव्र परिवर्तनों से ही परिलक्षित होती है। किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास की कुछ प्रमुख विशेषतायें निम्नवत् है-
1. भाव प्रधान जीवन- किशोरावस्था में किशोर-किशोरियों का जीवन अत्यधिक सहयोग आदि प्रवृत्तियाँ अधिक प्रबल होती है।
2. विरोधी मनोदशायें- किशोरावस्था में व्यक्ति में विरोधी मनोदशायें दिखाई देती है। लगभग समान परिस्थितियों में कभी वह अत्यधिक प्रसन्न तथा कभी अत्यन्त दुखी दिखाई देता है। जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से परिपूर्ण कर देती है, वही परिस्थिति किसी अन्य अवसर पर उसे खिन्न कर देती है।
3. संवेगों में विभिन्नतायें- किशोरावस्था में संवेगों में अत्यधिक विभिन्नतायें होती है। भिन्न-भिन्न अवसरों पर किशोर-किशोरियों के व्यवहार पर्याप्त भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं। वे कभी हतोत्साहित तथा कभी उत्साह से परिपूर्ण, कभी उत्साहीन, कभी अत्यधिक प्रसन्न तथा कभी अत्यधिकखिनन कभी अत्यधिक क्रोधी तथा कभी अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण, कभी अत्यधिक दयालु तथाकभी अत्यधिक रूष्ट दिखाई देते है।
4. काम भावना- किशोरावस्था में काम भावना व्यवहार के केन्द्रीय तत्व के रूप में कार्य करती है। काम भावना की तीव्रता के कारण किशोर-किशोरियों में प्रेम बढ़ जाते है। स्व प्रेम, समलिंगी प्रेम तथा विषमलिंगी प्रेम के रूप में किशोर- किशोरियों अपनी काम प्रवृत्ति की संवेगात्मक अभिव्यक्ति करते है।
5. वीर पूजा- किशोरावस्था में वीरपूजा की भावना विकसित हो जाती है। कल्पनाशील होने के कारण किशोर-किशोरियों को कहानी, उपन्यास सिनेमा, इतिहास तथा वास्तविक जवीन के अनुरूप किशोर-किशोरियों कुछ वीर-विरांगनाओं का चयन कर लेते है तथा उनके कार्यों व आदर्शों के अनुकरण करने का प्रयास करते है।
6. स्वाभिमान की भावना- किशोरावस्था में स्वाभिमान की भावना प्रबल होती है। किशोर-किशोरियां अपने आत्म गौरव, स्वाभिमान तथा सम्मान पर किसी प्रकार का आघात सहन करना नहीं चाहते है। स्वाभिमान पर चोट लगने पर कभी-कभी किशोर-किशोरी घर से पलायन कर जाते है अथवा आत्महत्या की बात सोचने लगते है।
7. अपराध प्र्रवृत्ति- किशोर को न तो बालक समझा जाता है तथा न ही पैठ जिसके कारण उसे समायोजन करने तथा संवेगात्मक व्यवहार में तरह-तरह की कठिनाइयेां का सामना करना पड़ता है। वातावरण से अनुकूलन करने के प्रयास में यदि असफलता मिलती है तो प्रायः उसमें निराशा की भावना विकसित होने लगती है। जो उसे अपराध प्रवृत्ति की ओर जीवन प्रवृत्त करती है। प्रेम का अभाव, इच्छापूर्ति में बाधा, निराशा से युक्त जीवन तथा नवीन अनुभवों की ललक के कारण किशोरावस्था में कभी-कभी अपराध प्रवृत्ति विकसित होने लगती है।
8. चिन्तामुक्त व्यवहार- किशोरावस्था में किशोर-किशोरियाँ अनेक बातों के प्रति चिन्तित रहते है वह अपने रंग, रूप, स्वास्थ्य, मान-सम्मान आर्थिक स्थिति सामाजिक स्वीकृति शैक्षिक प्रगति भावी व्यवसाय आदि के प्रति सदैव न केवलसजग वरन् त्त्यग्र रहते है।
9. स्वतन्त्रता की भावना- किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना अत्यधिक प्रबल होती है। किशोर-किशोरियां अपने परिवार तथा समाज के आदर्शों, परम्पराओं रीति-रिवाजों, अंधविश्वासों आदि को न मानकर अपनी स्वतंत्र जीवन शैली अपनाना चाहते है। वे तर्क-वितर्क रीति-रिवाजों तथा सामाजिक आदर्शोंं की उपयुक्तता को जानना चाहते है। यदि इसके क्रिया-कलापों पर प्रतिबन्ध लगाये जाते है तब किशोर इन्हें सरलता से स्वीकार नहीं करते, वरन् विद्रोह करने का प्रयास करते है। किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास के अवलोकन से स्पष्ट है कि किशोर में क्रियाशीलता तथा स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति अधिक होती है। जिसके परिणामतः इस अवस्था में संवेग प्रायः कुछ अधिक उग्र होते है। व्यक्ति के संवेगात्मक व्यवहार पर उसकी मानसिक क्षमता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों का संवेगात्मक क्षेत्र विस्तृत होता है। उच्च मानसिक क्षमता वाले बालकों में अपने संवेगों को नियंत्रित करने का अधिक क्षमता होती है। परिवार के वातावरण तथा सदस्यों का संवेगात्मक व्यवहार भी बालकों के संवेगात्मक विकास को तीन ढंग से प्रभावित करता है। प्रथम यदि परिवार में शान्ति सुरक्षा व स्नेह का वातावरण होता है तो बालक का संतुलित ढंग से संवेगात्मक विकास होता है। द्वितीय यदि परिवार मंे कलहपूर्ण, अत्यधिक सामाजिक तथा मौज-मस्ती का वातावरण रहता है तो, बालकों में अत्यधिक संवेग उत्पन्न हो जाते है। तृतीय यदि परिवार के सदस्य अतयधिक संवेदनशील होते हैं तथा प्रचुरता से संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो बालक भी अत्याधिक संवेदनशील होकर संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते है तो बालक भी अत्याधिक संवेदनशील होकर संवेगात्मक व्यवहार करते है। मानव जीवन में संवेगों से होता है तथा शिक्षा का सम्बन्ध व्यवहार के परिशोधन से होता है। इसलिए बालकों के संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करना शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है। माता-पिता तथा अध्यापकों को बालकों के संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करने तथा वांछित संवेगों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जाने चाहिए। बालकों के वातावरण को इस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए कि एक ओर जहाँ उनमें अवांछित, संवेगों को उदय न हो सके, वहीं दूसरी ओर उनमें वांछित संवेगों का संचार हो सके। शोधन अध्यवसाय तथा रेचन के द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। शोधन में अवांछित संवेगों को परिमार्जित करके उन्हें अच्छी दिशा दी जा सकती है। वैसे क्रोध की वृत्ति को शत्रुओं की ओरया काम प्रवृत्ति को साहित्य की ओर परिवर्तित किया जासकता है। अध्यवसाय में रत रहना, संवेगों को वशीभूत करने का एक अच्छा उपाय है। रेंचन का तात्पर्य है कि संवेगों को आने से रोका न जाये वरन् संवेगों को अभिव्यक्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाए। निःसन्देह अध्यापक तथा अभिभावकगण बालकों के संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे- नाटक खेल, स्काउटिंग, भ्रमण आदि के माध्यम से भी छात्रों का उचित ढंग से संवेगात्मक विकास किया जा सकता है।
(द) किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास- किशोरावस्था में एक बार फिर संवेगात्मक सन्तुलन बिगड़ जाता है। इस समय संवेगों में आँधी और तूफान की सी गति और प्रचण्डता होती है। इसलिए किशोरावस्था को प्रायः तूफान और तनाव का समय माना जाता है। जीवन की किसी अन्य अवस्था में संवेगात्मक शक्ति का प्रवाह इतना भीषण नहीं होता जितना कि इस अवस्था में पाया जाता है। एक किशोर के लिए अपने संवेगों पर नियन्त्रण रखना बहुत कठिन होता है। वे संवेगात्मक दृष्टिकोण से बहुत चंचल और अस्थिर हो जाते है। शिशु की तरह किशोर क्षण में रूष्ट और क्षण में तुष्ट दिखाई देते हैं। जरा सी बात पर बिगड़ पडना उत्तेजित हो जाना, आदि किशोरों के संवेगात्मक व्यवहार की सामान्य विशेषताएँ है।
हैडो रिपोर्ट ने इस आवश्यकता को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया है- ”युवाओं की धमनियों में 11 से 12 वर्ष की अवस्था से ही एक ज्वार उमड़ना प्रारम्भ हो जाता है, इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यह ज्वार बाढ़ का रूप धारण कर सकता है परन्तु अगर इस प्रचण्ड जल प्रवाह की पूरी शक्ति के साथ अनुकूल दिशा में प्रवाहित किया जाए तो यह अपने निश्चित लक्ष्य पर पहुँच सकता है।
1.1.7 संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक
1. स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास- शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य का संवेगात्मक विकास के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध है। आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शारीरिक न्यूनताएं कई प्रकार की संवेगात्मक समस्याओं को जन्म दे सकती है। संतुलित संवेगात्मक विकास के लिए विभिन्न ग्रन्थियों का ठीक प्रकार काम करना अत्यन्त आवश्यक है जो केवल स्वस्थ एवं ठीक ढंग से विकसित होते हुए शरीर में ही सम्भव हो सकता है।
2. बुद्धि- समायोजन करने की योग्यता के रूप में बालक के संवेगात्मक समायेाजन और स्थिरता की दशा में बुद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेल्टजन ने कहा है कि ”सामान्य रूप से अपनी ही उम्र के कुशाग्र बालकों की अपेक्षा निम्न बुद्धि स्तर के बालकों में कम संवेगात्मक संयम पाया जाता है। विचार शक्ति, तर्क शक्ति आदि बौद्धिक शक्तियों के सहारे ही व्यक्ति अपने संवेगों पर अंकुश लगाकर उनको अनुकूल दिशा देने में सफल हो सकता है। अतः प्रारम्भ से ही बच्चों की बौद्धिक शक्तियॉं बच्चे कमे संवेगात्मक विकास को दिशा प्रदान करने में लगी रहती है।“
3. पारिवारिक वातावरण और आपसी सम्बन्ध- परिवार के वातावरण और आपसी सम्बन्धों का भी बच्चे के संवेगात्मक विकास के साथ गहरा सम्बन्ध है जो कुछ बडे करते हैं उसकी छाप बच्चों पर अवश्य पड़ती है। अतः परिवार में बड़ों को जैसा संवेगात्मक व्यवहार होता है बच्चे भी उसी तरह का व्यवहार करना सीखा जाते है।
4. विद्यालय का वातावरण और अध्यापक- विद्यालय का वातावरण भी बालकों के संवेगात्मक विकास पर पूरा-पूरा प्रभाव डालता है। स्वस्थ और अनुकूल वातावरण के द्वारा बच्चों को अपना संवेगात्मक संतुलन बनाये रखने और अपना उचित समायोजन करने में बहुत आसानी होती है। विद्यालय के वातावरण में व्याप्त सभी बातें, जैसे विद्यालय की स्थिति उसका प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश, अध्यापन का स्तर, पाठान्तर क्रियाओं और सामाजिक कार्यों की व्यवस्था और अध्यापकों का स्वंय का संवेगात्मक व्यवहार आदि बालकों के संवेगात्मक विकास को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। संवेगात्मक कारक के बाद अब हम संवेगात्मक बुद्धि का प्रकाश डालते है।
संवेगात्मक बुद्धि
संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग 1990 में सबसे पहले दो अमेरिकन प्रोफेसरों डॉ0 जॉन मेयर तथा डॉ0 पीटर सेलोवे द्वारा एक ऐसा वैज्ञानिक प्रमाप तैयार करने हेतु किया गया था जिससे लोगों की संवेगात्मक क्षेत्र में विद्यमान वैयक्तिक योग्यताओं में विभेदीकरण किया जा सके। परन्तु जिस रूप में आज संवेगात्मक बुद्धि पद की सर्वत्र चर्चा की जाती है, उसे इस तरह से लोकप्रिय बनाने का श्रेय केवल मात्र एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को ही जाता है। उन्होंने अपनी 1995 में प्रकाशित एक पुस्तक ”संवेगात्मक बुद्धि: बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों“ के माध्यम से इसे विशेष चर्चा का विषय बनाया है।
संवेगात्मक बुद्धि पद को कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किये गये प्रयत्नों तथा प्रदत्त परिभाषाओं के आधार पर भली-भांति समझा जा सकता है।
”संवेगात्मक बुद्धि को एक ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे चार विभिन्न रूपों में संवेगों को उचित दिशा देेने में मदद मिले जैसे संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना, उसका अपनी विचार प्रक्रिया में समन्वय करना, उसे समझना तथा उसका प्रबन्धन करना।“
यह परिभाषा बताती है कि हम सभी ने अपने संवेगों से निपटने हेतु अलग-अलग ढंग की क्षमता और योग्यता पाई जाती है और उसी के अनुरूप एक समूह में दूसरों की तुलना में किसी भी व्यक्ति विशेष की संवेगात्मक बुद्धि की दृष्टि से अधिक या कम बुद्धिमान माना जाता है।
एक व्यक्ति को उतना ही संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान माना जाता है जितनी कि क्षमता और योग्यता वह निम्न रूपों में प्रदर्शित करता है।
संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति विशेष की उस समग्र क्षमता से है जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरों के संवेगों को जानने, समझने तथा उनकी ऐसी उचित अनुभूति एवं अभिव्यक्ति करने कराने में इस प्रकार मदद करें कि वह ऐसी वांछित व्यवहार अनुक्रियायें करसके जिनसे उसे दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपना समुचित हित करने हेतु अधिक से अधिक अच्छे अवसर प्राप्त हो सके।
संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता एवं महत्व
व्यक्ति की सभी प्रकार की सफलताओं के पीछे पूरी तरह किसी न किसी रूप में उसकी मानसिक योग्यताओं तथा क्षमताओं का ही हाथ रहता है और इसलिए सामान्य बुद्धि की मात्रा यानी आई क्यू को एक ऐसा आधार माना जाता था जिससे यह भविष्यवाणी की जा सके कि व्यक्ति विशेष किसी कार्य विशेष के सम्पादन में किस सीमा तक सफल होगा। परन्तु इस धारणा का वर्चस्व मनोविज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम अनुसंधानों ने लगभग समाप्त सा ही कर दिया है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉ0 डेनियल गोलमैन का बहुचर्चित पुस्तकों ने संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता एवं महत्व को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से जनमानस के समक्ष रखने का प्रयत्न किया है। संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में व्यक्त गोलमैन के इन विचारों को संक्षेप में लिपिबद्ध किया जा सकता है।
संवेगात्मक बुद्धि के लिये सामान्य बुद्धि की तुलना में एक बात यह भी अधिक महत्वपूर्ण है कि इसे संवेगात्मक क्षमताओं में वृद्धि कर वांछित रूप से विकसित करने के प्रयास किये जा सकते है और फिर इस विकास के माध्यम से व्यक्तियों को अपना जवीन सुखमय और शांतिप्रद बनानेे में सहायता की जा सकती है।
संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा को मात्र इसलिए नहीं सराहा जा सकता है कि यह एक नवीनतम अवधारणा है बल्कि इसलिये कि यही एक ऐसी अवधारणा है जो बालकों और हम सभी के सामने आदर्श रखती है कि किस प्रकार हम अपने आपको समर्थ बनाये तथा सुखी रहे।
संवेगात्मक बुद्धि के बारे में डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विचारों ने एक तरह से हमारे जीवन के विविध क्षेत्रों में संवेगात्मक बुद्धि की आवश्यकता एवं उपयोग को लेकर एक क्रांति सी मचा दी है।
1.1.10 संवेगात्मक बुद्धि का मापन
सामान्य बुद्धि के मापन हेतु हम किसी न किसी प्रकार के बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करते है उसी रूप में संवेगात्मक बुद्धि की जाँच हेतु हमें भली-भांति निर्मित परीक्षणों जैसे संवेगात्मक बुद्धि परीक्षणों या स्कूलों काप्रयोग कर सकते है। उदाहरण स्वरूप कुछ उपलब्ध परीक्षणों का निम्न प्रकार उल्लेख किया जा सकता है।
1. मेयर इमोशनल इन्टैलीजैन्स स्केल इसे अमेरिका की न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉ0 जान मेयर द्वारा बनाया गया है।
2. बार ऑन इमोशनल कोशेन्ट इनबेन्टरी अमेरिका के डॉ0 रॅयूबेन बार ऑन द्वारा निर्मित एवं मल्टी हैल्थ सिस्टम यू0एस0ए0 द्वारा प्रकाशित।
माध्यमिक स्तर के अध्यापक स्नातक शिक्षा प्राप्त होते है तथा इन्होंने बी0एड0 अथवा एल0टी0 प्रशिक्षण प्राप्त किया होताहै। उच्च माध्यमिक स्तर के अध्यापक स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त होते हैं परन्तु इनके लिए प्रायः किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। बी0एड0 पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों के द्वारा संचालित किया जाता है तथा इनकी कक्षायें विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षा विभागों तथा शिक्षा महाविद्यालयों में आयोजित की जाती हैं। यह एक वर्षीय पाठ्यक्रय है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के बी0एड0 पाठ्यक्रमों में प्रश्नपत्रों की संख्या, प्रकृति व विषयवस्तु के सम्बन्ध में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है, फिर भी मोटे तौर पर बी0एड0 शिक्षा के दर्शानिक व समाजशास्त्रीय पक्ष, मनोविज्ञान, शिक्षा तकनीकी, मापन व मूल्यांकन, विषय शिक्षण विधि, विद्यालय प्रशासन, स्वास्थ्य शिक्षा का सैद्धान्ति ज्ञान तथा शिक्षण अभ्यास कराया जाता है। देश के कई विश्वविद्यालय पत्राचार तथा ग्रीष्मकालीन बी0एड0 जैसे पाठ्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। सेवारत अध्यापकों के लिए भी बी0एड0 के कुछ विशेष पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। ये सारा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0) की देखरेख में पूरा किया जाता है।